Post Contents
अष्टांग योग / Ashtanga YOGA
योगसूत्र के जनक पतंजली ने अष्टांग योग की परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की है। इन्होने योग के सभी अंगो को मिलाकर अष्टांग योग का रूप दिया। अष्टांग योग का अर्थ है योग के आठ अंग जिन्हे मिलाकर अष्टांग योग बना है।
योगांगनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः
अर्थ – योग के अंग का अनुष्ठान ( प्रयोग,क्रियात्मक रूप ) करने से अशुद्धि का नाश होकर ज्ञान का प्रकाश और विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है |
अष्टांग योग क्या है ?

महर्षि पतंजलि को योग का पिता भी कहा जाता है | ईशा से 200 वर्ष पूर्व ही महर्षि पतंजलि ने योग के आठों अंगो को मिलाकर योगसूत्र का निर्माण कर दिया था | अष्टांग योग में योग के आठ अंग आते है (यम,नियम,आसन,प्राणायाम,प्रत्याहार,धारणा,ध्यान और समाधी ) | आप इसे इस परिभाषा तरह भी समझ सकते है कि योग के आठों आयामों को अपनाकर मोक्ष को प्राप्त होना ही अष्टांग योग है |
अष्टांग योग के अंग
अष्टांग योग के 8 अंग है और हरेक अंग का अपना कार्य और महत्व है जिसे अपना कर व्यक्ति पूर्ण रूप से साक्षात् मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है | इस योग में अलग – अलग आयामों को एक साथ अपनाकर अभ्यास किया जाता है जो पूर्ण रूप से फलित होते है | इन 8 अंगो की दो भूमिकाएँ होती है
- बहिरंग – यम,नियम,आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन पांच अंगो को बहिरंग कहते है क्योंकि इनकी विशेषता शरीर के बाहर की क्रियाओं से ही सम्बंधित होती है |
- अन्तरंग – धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनो अंगो को अन्तरंग कहते है क्योंकि इनका सम्बन्ध केवल अंत:करण से ही होता है | इसी कारण इन अंगो को अन्तरंग कहा जाता है|
यम
यम का अर्थ होता है नैतिकता | जैन धर्म में बताये गए अहिंसा, सत्य, अस्तेय(चोरी न करने का भाव) , ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न करना) इन नियमो को ही यम कहा गया है | योग में इन्ही नियमो का पालन करके योग साधना करना ही यम कहलाता है |
नियम
अष्टांग योग में नियम का अर्थ होता है शौच,संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधाम | अष्टांग योग के प्रत्येक साधक के जीवन में ये नियम होने जरुरी है | साधक को किसी दुसरे के विषय में गलत सोच राग द्वेष और इर्ष्य का भाव नही रखना चाहिए | उसे संतोष रखना और अपने तप के माध्यम से मानसिक अशुद्धियों को दूर करना चाहिए | इसी प्रकार स्वाध्याय और इश्वर के समक्ष साक्षी होकर अपने अहम को त्यागना भी नियम के अंतर्गत आता है |
आसन
महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का तीसरा अंग आसन है सुखपूर्वक स्थिर बैठने का नाम आसन है | जिस क्रिया से स्थिरतापूर्वक निराकुलता के लिए सुखपूर्वक दीर्घकाल तक बैठा जा सके वह आसन कहलाता है | योगी आसनों के निरंतर अभ्यास से शरीर और अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है | आसन-सिद्धि हो जाने से साधक हर प्रकार के क्लेश से मुक्ति पा लेता है
प्राणायाम
अष्टांग योग में प्राणायाम का एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है | आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास-प्रश्वास की गति का विच्छेद होना ही प्राणायाम कहलाता है | यहाँ श्वास का अर्थ प्राणवायु को नासिका के माध्यम से अन्दर प्रवेश करवाना और प्रश्वास का अर्थ है कोष्ठ में स्थित वायु को नासिका के द्वारा शरीर से बाहर निकालना |
प्रत्याहार
प्रत्याहार का अर्थ होता है अपनी पांचो इन्द्रियों को अपने वश में करना ही प्रत्याहार है | प्राणायाम से सभी इन्द्रियां धीरे-धीरे शुद्ध होने लगती है और वे बाहरी भोगों का त्याग करने में सक्षम हो जाती है | प्रत्याहार के माध्यम से हरेक इन्द्रिय को उनके विषयों से अलग करके उन्हें एक स्वरुप करना होता है | आसन और प्राणायाम की सिद्धि के बाद अपने मानसिक विकारों को हटाकर अपने मूल स्वरुप में स्थित होना ही प्रत्याहार कहलाता है |
आप प्रत्याहार को सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते है जैसे हमारी पांच इन्द्रियां – आँख , कान , नाक , जीभ, और जीभ | ये इन्द्रियां अपने विषयों को देख कर मोहित होती है और उनका स्वाद चखने को तत्पर रहती है जैसे – स्वादिष्ट पकवान के लिए जीभ लालायित रहती है | लेकिन इन इन्द्रियों की आसक्ति के पीछे भी मुख्य भूमिका हमारे मन की होती है | प्रत्याहार में साधक को अपनी इन्द्रियों को उनके विषयों से विमुख करके अंतरात्मा की और मोड़ना होता है |
धारणा
धारणा का अर्थ होता है अपने चित की वर्ती को देश (स्थान) विशेष में बंधना ही धारणा कहलाती है | धारणा में साधक को अपने मन को एकाग्रचित करना होता है और परमेश्वर के ध्यान में मन को लगाना होता है |
ध्यान
साधक के द्वारा मन को एकाग्र और एकतान करना ही ध्यान कहलाता है | धारणा से शुद्ध हुए चित को ध्यान में लगाकर अपने मन और आत्मा को एकाग्र और चंचलताहीन बनाया जा सकता है |
समाधी
जब निरंतर ध्यान के द्वारा हमारा मन और आत्मा में ध्यये का मात्र ध्यान रहे और सारा शरीर शून्य मात्र हो जाए यह स्थिति समाधी कहलाती है | अष्टांग योग के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है | ध्यान की अंतिम स्थिति को समाधी कहा जाता है | इस स्थिति में आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है | अष्टांग योग के साधक की यह अंतिम खोज होती है | इसके बाद सिर्फ शुन्य रह जाता है |
अष्टांग योग के महत्व या फायदे
यदि हम गहराई से देखें तो योग के आठ अंग कोई साधारण कार्य नहीं करते बल्कि इनका कार्य तो आत्मा से परमात्मा करना है | हमारे ऋषि-मुनियों ने योग को अलग – अलग बाँट कर फिर इन्हें एक सूत्ररूप में पिरोया ताकि व्यक्ति इन आठों अंगो के अलग – अलग कार्यों के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मोक्ष तक को प्राप्त कर सके | अष्टांग योग को अपना कर हम स्वस्थ ही नहीं इस घोर जन्म – मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्ति पा सकते है |
धन्यवाद |
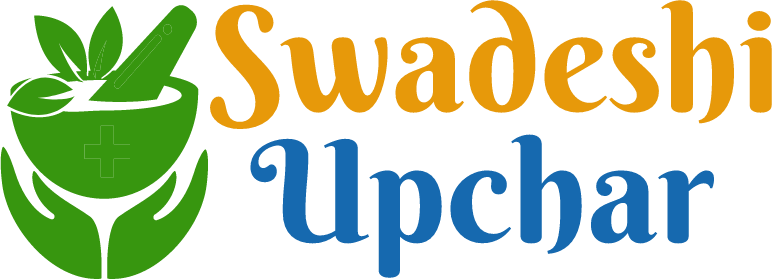
Thanks for the amazing tips, really helpful information